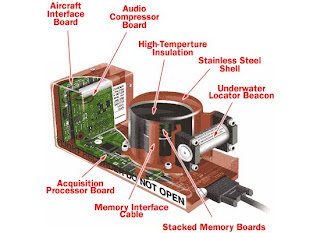भागदौड़ भरे इस माहौल में न तो लोगों के खाने का समय तय है, न सोने का। एक्सर्साइज करना तो दूर, समय की दुहाई देकर वे दफ्तर की सीढि़यां चढ़ने से भी परहेज करते हैं। तनाव इस कदर हावी है कि सपने में भी या तो ड्राइविंग करते रहते हैं या दफ्तर की फाइलें पीछा नहीं छोड़तीं। ऐसे में कई बीमारियां चुपके से घर कर जाती हैं। ऐसी ही एक बीमारी है पेप्टिक अल्सर, जो शरीर में ज्यादा एसिडिटी की वजह से होती है।
क्या होता है पेप्टिक अल्सर
पेप्टिक अल्सर एक ऐसी स्थिति है, जिसमें पेट की अंदरूनी दीवारों पर छाले पड़ जाते हैं। बीमारी बढ़ जाने पर ये छाले गहरे घाव में बदल जाते हैं और मरीजों को ज्यादा परेशानी होने लगती है। गलत खानपान की वजह से जब पेट में एसिड ज्यादा बनने लगता है तो यह स्थिति पैदा हो जाती है। यह बीमारी बैक्टिरिया के इंफेक्शन की वजह से भी होती है।
एसिड रिफ्लक्स डिजीज
जब हम भोजन करते हैं तो आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है, जिससे भोजन का पाचन होता है। बदहजमी की वजह से कभी-कभी एसिड ऊपर की ओर आहार नली में चला जाती है। इससे जलन महसूस होती है। इसका असर गले, दांत, सांस आदि पर पड़ने लगता है। इससे सांस लेने में तकलीफ बढ़ जाती है, आवाज भारी हो जाती है और मुंह में छाले पड़ जाते हैं। इस तरह की स्थितियों को एसिड रिफ्लक्स डिजीज कहा जाता है।
कितनी तरह का अल्सर
गैस्ट्रिक अल्सर : इसमें भोजन के बाद पेट में दर्द होने लगता है। डाइजीन जैसी दवाएं लेने के बाद आराम मिल जाता है।
ड्यूडिनल अल्सर : खाली पेट रहने से दर्द होता है। भोजन करने के बाद दर्द ठीक हो जाता है। अगर 15 लोगों को ड्यूडेनल अल्सर होता है तो मुश्किल से 1 या 2 लोग गैस्ट्रिक अल्सर के शिकार होते हैं।
इसोफेगल अल्सर : इसमें आहार नली के निचले हिस्से में छाले पड़ जाते हैं या छिद्र हो जाते हैं। इससे आहार नली में तेज जलन होती है।
पेप्टिक अल्सर की वजह
एसिड की अधिकता : पेट में ज्यादा मात्रा में एसिड बनना पेप्टिक अल्सर की मुख्य वजह है। इसके लिए ज्यादा मिर्च-मसाले वाला खाना और गलत खानपान जिम्मेदार है।
एच-पायलोरी इंफेक्शन : 1980 में एक ऑस्ट्रेलियाई वैज्ञानिक ने एच-पायलोरी (हेलिकोबेक्टर पायलोरी) नामक बैक्टिरिया का पता लगाया था। उन्होंने माना था कि सिर्फ खान-पान और पेट में एसिड बनने से पेप्टिक अल्सर नहीं होते, बल्कि इसके लिए एक बैक्टिरिया भी दोषी है। इसका नाम एच-पायलोरी रखा गया। एंडोस्कोपी से इसकी स्थिति का पता चलता है। पेप्टिक अल्सर के लिए एच-पायलोरी बैक्टिरिया जिम्मेदार है, फिर भी 90 फीसदी लोगों के पेट में इस बैक्टिरिया के होने के बावजूद उनमें अल्सर नहीं होता। 10 फीसदी लोगों में इस बैक्टिरिया के होने के बावजूद अल्सर होता है।
पेनकिलर्स का इस्तेमाल : कई पेनकिलर्स और बुखार उतारने की दवाएं नॉन-स्टिरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स (एनएसएआईडी) की कैटिगरी में आती हैं। इनमें एस्प्रिन, आइब्रुफेन और नेप्रेक्सिन समूह की दवाएं प्रमुख हैं। इन दवाओं को ज्यादा लेने से एसिड बनता है।
तनाव : तनाव की वजह से एसिड ज्यादा बनता है। बाद में यही पेप्टिक अल्सर का रूप ले लेता है।
स्मोकिंग : स्मोकिंग पेप्टिक अल्सर की एकमात्र वजह नहीं है, लेकिन यह अल्सर के जोखिम को बढ़ा देता है। स्मोकिंग की वजह से अल्सर की दवा का असर कम हो जाता है।
लक्षण
पेट के ऊपरी हिस्से में तेज दर्द होना अल्सर का लक्षण हो सकता है।
भोजन के बाद जब पेट में दर्द हो और डाइजिन जैसी एंटी-एसिड दवाओं से राहत मिले तो इसे गैस्ट्रिक अल्सर का लक्षण माना जाता है।
ड्यूडिनल अल्सर में खाली पेट दर्द होता है और भोजन के बाद दर्द से राहत मिलती है। अक्सर इसका दर्द रात को होता है।
अगर दर्द छाती के पास हो तो इसे एसिडिटी रिफ्लेक्शन का असर समझना चाहिए। इससे दिल के दर्द का शक होता है। दिल का दर्द छाती के ऊपरी हिस्से में होता है और कभी-कभी एसिडिटी की वजह से भी उसी जगह दर्द होता है, इसलिए बिना जांच के अंतर समझ पाना आसान नहीं है।
पेप्टिक अल्सर होने से मरीज को भूख कम लगती है। सामने खाना होने पर भी खाने की इच्छा नहीं होती।
उलटी होना या उलटी जैसा महसूस होना अल्सर का लक्षण माना जा सकता है। जब अल्सर बढ़ जाता है, तो खून की उलटी हो सकती है। ऐसे में स्टूल (मल) का रंग काला हो जाता है।
अल्सर से बचाव
रेशे वाला भोजन लें और मिर्च-मसाले का इस्तेमाल कम करें।
चाय, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक्स, जंक फूड कम लें।
खाना समय पर और तसल्ली से खाएं।
टेलिविजन देखते हुए खाना न खाएं।
रात के खाने और सोने के बीच कम-से-कम दो घंटे का अंतर होना चाहिए।
जूस, लस्सी या मीठे तरल पदार्थ पीने में लोग जल्दबाजी करते हैं। यह गलत है। ऐसी चीजों को धीरे-धीरे पीना चाहिए। धीरे-धीरे पीने से मुंह का सलाइवा इसमें मिल जाता है, जिससे ये चीजें जल्दी पच जाती हैं।
स्मोकिंग से परहेज करें।
तनावमुक्त रहने की कोशिश करें।
नियमित व्यायाम करें।
दवाएं डॉक्टरों की सलाह से ही लें।
अगर अल्सर हो जाए, तो एनएसएडी समूह की दवा न लें।
पेनकिलर्स के रूप में क्रोसिन का इस्तेमाल किया जा सकता है।
क्या है इलाज
1. एलोपैथी
एंटी-अल्सर किट : पेप्टिक अल्सर में 10 दिन की दवा दी जाती है। इसे एंटी-अल्सर किट कहते हैं। इसमें खासतौर से पीपीआई (प्रोटॉन पंप इनहिबिटर), क्लैरीथ्रोमाइसिन और एमॉक्सिस्लिन ग्रुप की दवाएं होती हैं। इनसे एसिड का असर कम हो जाता है। मरीज को ये दवाएं डॉक्टर द्वारा बताए गए परहेज के साथ लेनी चाहिए।
ऑपरेशन : पहले पेप्टिक अल्सर की वजह से ब्लड आने की स्थिति में ऑपरेशन करने की जरूरत पड़ती थी, लेकिन अब एंडोस्कोपी की मदद से इलाज किया जाता है।
क्या है एंडोस्कोपी
एंडोस्कोपी एक ऐसी प्रक्रिया है, जिसमें शरीर के अंदरूनी हिस्सों के बारे में एंडोस्कोप की मदद से पता लगाया जाता है। एंडोस्कोप पतला लचीला ट्यूब होता है, जिसके एक सिरे पर रोशनी की व्यवस्था होती है और इसमें विडियो कैमरा लगा होता है। इसकी मदद से कंप्यूटर स्क्रीन पर शरीर के भीतरी हिस्सों की तस्वीरें देखी जाती हैं। पेप्टिक अल्सर के मामले में इसे मुंह के रास्ते या मलद्वार से शरीर में प्रवेश कराया जाता है। इसका इस्तेमाल मरीज को बिना बेहोश किए किया जाता है। जब अल्सर फट जाता है या अल्सर के घाव गहरे होकर धमनी को डैमेज कर देते हैं, तो एंडोस्कोप की मदद से खून के बहाव को रोका जाता है। उसके बाद दवा से इलाज किया जाता है।
2. होम्योपैथी
अर्सेनिकल एल्बम, फॉस्फोरस, सल्फर, आयरिस वर्सिकोलर, कैली बायक्रोमिकम, आर्जेंटम नाइट्र्किम, ग्राफिक आदी हैं।
इन दवाओं का चयन होम्योपैथी डॉक्टर की सलाह पर करना चाहिए। मरीज और मर्ज के इतिहास को बेहतर जानने के बाद ही डॉक्टर दवाओं का चयन करते हैं।
4. घरेलू उपचार
पोहा (बिटन राइस) और सौंफ को बराबर मात्रा में मिलाकर चूर्ण बना लें। 20 ग्राम चूर्ण को 2 लीटर पानी में सुबह घोलकर रख लें और रात में पूरा पी जाएं। रोज सुबह तैयार करें और दोपहर बाद या शाम से पीना शुरू कर दें। इस घोल को 24 घंटे में खत्म कर देना है।
दूध गैस्ट्रिक एसिड बनाता है, लेकिन आधा कप ठंडे दूध में आधा नीबू निचोड़कर पिया जाए तो वह पेट को आराम देता है। जलन का असर कम हो जाता है।
पत्ता गोभी और गाजर को बराबर मात्रा में लेकर जूस बना लें। सुबह-शाम एक-एक कप पीने से पेप्टिक अल्सर के मरीजों को आराम मिलता है।
गाय के दूध से बने कच्चे घी का इस्तेमाल फायदेमंद होता है।
बादाम पीसकर बनाए गए दूध से मरीज को काफी लाभ पहुंचता है।
ड्रम स्टिक (सहजन) के पत्ते को पीसकर दही के साथ पेस्ट बनाकर लें।
कुछ सवाल
क्या कम खाने से एसिड बनता है?
नहीं।
ज्यादा खाने से एसिड बनता है?
ज्यादा खाने से बदहजमी हो सकती है। ऐसे में पाचन क्रिया प्रभावित होती है।
ईनो के फायदे-नुकसान क्या हैं?
कोई नुकसान नहीं है, लेकिन इसे आदत नहीं बनानी चाहिए। इसे एसिड के असर को कम करने के लिए लिया जाता है। बेहतर यह है कि इसे ठंडे पानी में लिया जाए।
डायजीन, रेनटेक, ओमेज लेना नुकसानदायक है?
परेशानी होने पर इमर्जेंसी में इन दवाओं को लेना ठीक है, लेकिन इसकी आदत नहीं होनी चाहिए।
हाजमोला, पुदीन-हरा आदि का कोई नुकसान तो नहीं होता?
ये एक तरह के एंटी-एसिड हैं। इनसे राहत मिलती है। लेने में हर्ज नहीं है लेकिन बीमारी का पता लगाना जरूरी है।
ठंडा दूध या आइसक्रीम लेने के कुछ नुकसान तो नहीं हैं?
ये भी एंटी-एसिड का काम करते हैं। दूध से राहत तो मिलती है लेकिन बाद में यह अमाशय में गैस्ट्रिक एसिड का निर्माण करता है। यह हानिकारक है।
नॉन-स्टिरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स के साथ डॉक्टर एक टैब्लेट रात को खाने को देते हैं, जिससे गैस न बने। इस तरीके से इन ड्रग्स को लेना सही है क्या?
बिल्कुल सही है। इससे अल्सर नहीं होता।
क्या अल्सर से कैंसर हो सकता है
अल्सर से कैंसर होने की आशंका बहुत कम होती है। जितनी भी आशंका होती है, वह भी गैस्ट्रिक अल्सर की वजह से ही होती है। कभी-कभी ऐसा भी होता है कि कैंसर की वजह से अल्सर डिवेलप हो जाता है।